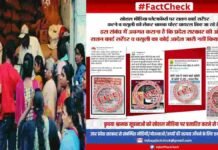- भारतीय समाज में जाति व्यवस्था सदियों से गहराई तक जड़ें जमाए हुए है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई बताते हुए कहा था, जाति व्यवस्था सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए घातक है। संदर्भ, अंबेडकर, Annihilation of Caste, 1936
- आज़ादी के बाद जब लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित हुआ, तो संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए। लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जाति अब भी राजनीतिक लामबंदी का सबसे मजबूत आधार बनी रही।
- 1950–60 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने जातीय संतुलन के आधार पर टिकट वितरण की राजनीति शुरू की। इसके बाद 1980 और 1990 का दशक मंडल आयोग और उसकी सिफारिशों संदर्भ: मंडल आयोग रिपोर्ट, 1980; लागू 1990 के बाद जातीय राजनीति का निर्णायक दौर साबित हुआ। समाजवादी पार्टी (सपा) ने यादवों और अन्य पिछड़ी जातियों को संगठित किया, तो बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने जाटवों और दलितों को एक राजनीतिक शक्ति में बदला।
- राजनीति विज्ञानी पॉल ब्रास (Paul Brass) और आंद्रे बेटेयल (Andre Béteille) ने अपनी रचनाओं में लिखा है कि भारतीय राजनीति में जाति सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि सत्ता का स्थायी औजार है। (Béteille, “Caste, Class and Power, 1965)
- सरकार का यह आदेश ऐसे समय आया है जब पंचायत चुनाव नज़दीक हैं। पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ‘जाति-प्रधान’ माने जाते हैं।
- 2015 और 2021 के पंचायत चुनावों के परिणाम दर्शाते हैं कि ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक उम्मीदवारों का चयन जातिगत समीकरणों पर आधारित होता है (संदर्भ: यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत चुनाव रिपोर्ट्स)।
- गाँव-कस्बों में वोटिंग पैटर्न इस कदर जाति-आधारित है कि उम्मीदवार अक्सर अपने जातीय समूह के मतदाताओं के दम पर जीत सुनिश्चित करते हैं।
- ऐसे में जातीय रैलियों पर रोक से पंचायत चुनावों का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है।
- जाति आधारित रैलियां, सम्मेलन और राजनीतिक आयोजन वर्जित होंगे।
- इंटरनेट व सोशल मीडिया पर जाति आधारित कंटेंट साझा नहीं किया जाएगा।
- प्रशासनिक और पुलिस अभिलेखों से जाति का उल्लेख हटाया जाएगा।
- सार्वजनिक स्थानों, वाहनों और साइनबोर्ड से जाति-सूचक प्रतीक व नारे हटाए जाएंगे।
- विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार बताया है।
- समाजवादी पार्टी का कहना है कि जाति पहचान को दबाना दरअसल पिछड़े वर्गों और दलितों की आवाज़ दबाना है।
- बहुजन समाज पार्टी के लिए तो यह सीधा झटका है, क्योंकि पार्टी की राजनीति ही दलित रैलियों और जनसभाओं पर टिकी है।
- विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने यह आदेश “पीडीए” (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) गठजोड़ के उभार को रोकने के लिए लाया है।
- इंटरनेट नियंत्रण: लाखों फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सऐप ग्रुप जातीय राजनीति पर सक्रिय हैं। प्रशासन इन्हें कैसे नियंत्रित करेगा?
- जमीनी हकीकत: गाँव-कस्बों में जाति सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों, शादियों और रोज़मर्रा के व्यवहार का हिस्सा है। इसे रैलियों या नारे हटाने भर से खत्म नहीं किया जा सकता।
- प्रशासनिक अभिलेख: पुलिस और प्रशासनिक दस्तावेज़ों से जाति का उल्लेख हटाना व्यावहारिक कठिनाई पैदा करेगा, क्योंकि कई सरकारी योजनाएं जाति-आधारित आरक्षण और लाभ पर टिकी हैं।
सकारात्मक प्रभाव जातीय नारे और प्रतीकों पर रोक से समाज में समरसता का माहौल बन सकता है। राजनीतिक दलों को जाति से ऊपर उठकर मुद्दा-आधारित राजनीति करनी होगी। युवाओं में जातीय पहचान की जगह रोजगार और विकास के मुद्दे केंद्र में आ सकते हैं।हाशिए पर खड़े समूहों की आवाज़ कमजोर हो सकती है।विपक्ष के लिए यह लोकतंत्र को एकरूपता में बदलने का प्रयास है।सोशल मीडिया पर पाबंदियों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठेंगे।
उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों पर रोक का आदेश एक साहसिक और विवादास्पद कदम है। यह समाज में समानता और समरसता लाने का दावा करता है, लेकिन इसके राजनीतिक निहितार्थ गहरे हैं।यह आदेश यदि सख्ती से लागू होता है तो जातीय राजनीति को हिला सकता है। लेकिन यदि यह केवल कागज़ी आदेश बनकर रह गया तो यह राजनीति की एक और ‘रणनीतिक चाल’ माना जाएगा।अंततः, असली सवाल यही है, क्या सचमुच जाति को राजनीति से अलग किया जा सकता है?या यह आदेश भी लोकतंत्र की उस खींचतान का हिस्सा है जहां सत्ता की मजबूरी और समाज की वास्तविकता टकराती है?
देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते है