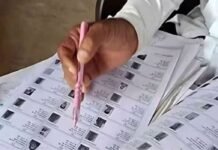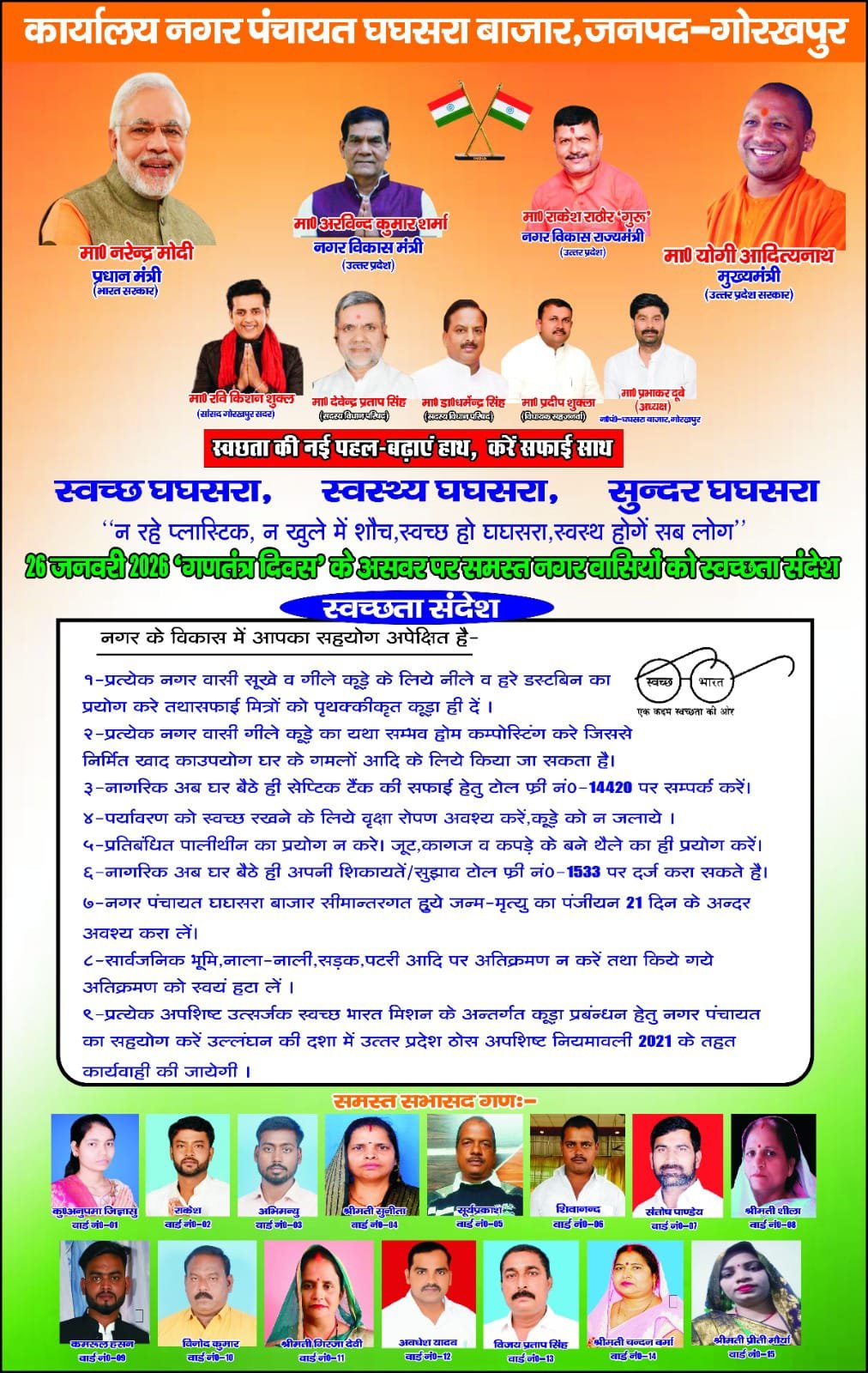भारतीय साहित्य के इतिहास में 31 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन दो महान साहित्यकारों गोस्वामी तुलसीदास (Goswami Tulsidas) और मुंशी प्रेमचंद (Munshi Premchand) का जन्म हुआ। एक ने भक्ति युग में रामकथा को जन-जन तक पहुँचाया, दूसरे ने नवजागरण काल में समाज के यथार्थ को शब्द दिए। तुलसीदास ने जहां अध्यात्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया, वहीं प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त असमानता, शोषण और अन्याय के विरुद्ध कलम चलाई। यद्यपि दोनों की भाषा, काल, शैली और दृष्टिकोण भिन्न रहे, लेकिन दोनों की लेखनी का मूल उद्देश्य एक ही था, जनमंगल और समाज सुधार। यह लेख तुलसीदास और प्रेमचंद के जीवन, रचनाओं, ऐतिहासिक संदर्भों और उनके विचारों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।
गोस्वामी तुलसीदास

गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत् 1589 (ईस्वी 1532) में उत्तर प्रदेश के बाँदा ज़िले के राजापुर गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी थीं। बचपन में ही माता-पिता का साया उठ गया। उनके जीवन की सबसे प्रसिद्ध किंवदंती यह है कि जन्म के समय वे बारह महीने के भ्रूण थे और उनके मुख से “राम” नाम निकला था, जिससे लोग भयभीत हो गए। उनका लालन-पालन एक साधु श्री नरहरिदास ने किया। युवावस्था में विवाह हुआ, लेकिन पत्नी रत्नावली के कटाक्ष ,’लाज न आवत आपको दौरे अति अधम अस देह, धन्य-धन्य वे पितु मातु जिनकी तुम अनुराग।’ ने उन्हें जीवन की दिशा बदलने को विवश किया। इसके बाद वे रामभक्ति में लीन हो गए।
मुख्य रचनाएँ

तुलसीदास की रचनाओं ने न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि जन-जन के मानस पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं:
- रामचरितमानस (अवधी भाषा में)
- हनुमान चालीसा
- विनय पत्रिका
- कवितावली
- दोहावली
- जानकी मंगल
- रामलला नहछू
रामचरितमानस

तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जिसे वे “श्रवण काव्य” कहते थे। इस ग्रंथ में उन्होंने संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण को अवधी भाषा में सरल, भक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि यह ग्रंथ आज भी घर-घर में पढ़ा जाता है।
हनुमान चालीसा

इस 40 छंदों के स्तोत्र में भक्ति, बल और समर्पण की भावना कूट-कूटकर भरी है। यह तुलसीदास की सरलता और लोकव्यवहार के प्रति जागरूकता को दर्शाता है।
तुलसीदास की विचारधारा
तुलसीदास राम को केवल एक राजा नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्श का प्रतीक मानते थे। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि-
“धर्म न दूजा सत्य समाना।
परहित सरिस धर्म नहि भाई,
परपीड़ा सम नहि अधमाई।”
तुलसीदास के समय समाज में मुस्लिम शासन, जातिगत विघटन और धर्म को लेकर भ्रम फैला हुआ था। उन्होंने रामकथा के माध्यम से लोगों को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी।
ऐतिहासिक महत्त्व
तुलसीदास ने भाषा का लोककरण किया। जब संस्कृत केवल ब्राह्मणों की भाषा थी, उन्होंने अवधी जैसी जनभाषा में रचनाएँ कर आम जन को सीधे जोड़ा। यह एक प्रकार का धार्मिक लोकतंत्रीकरण था। उन्होंने भगवान को मंदिरों से निकालकर लोक-मन में स्थापित किया।
प्रसिद्ध उद्धरण
‘राम नाम बिनु गति नहिं कोई।’
‘समरथ को नहीं दोष गोसाईं।’
‘भय बिनु होइ न प्रीति।’
‘सीय राममय सब जग जानी।’
‘तुलसी मस्तक तब नवा, धनुष-बाण ले राम।’
मुंशी प्रेमचंद

मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस ज़िले के लमही गाँव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने उर्दू में ‘नवाब राय’ नाम से लेखन प्रारंभ किया। उनके पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बाल्यकाल में माता-पिता का देहांत हो गया।कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने शिक्षक की नौकरी की और फिर हिंदी तथा उर्दू साहित्य को समर्पित हो गए। जीवन के उत्तरार्ध में ‘हंस’ पत्रिका का संपादन किया और लेखन को ही आजीविका का साधन बनाया।
प्रमुख रचनाएँ

उपन्यास
- गोदान — भारतीय किसान की त्रासदी पर आधारित उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास
- गबन — उपभोक्तावाद और नैतिक द्वंद्व
- कर्मभूमि — स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में
- निर्मला — दहेज और स्त्री शोषण पर
- सेवासदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, वरदान आदि
कहानियाँ

- कफन
- ईदगाह
- पूस की रात
- सद्गति
- बड़े भाई साहब
- ठाकुर का कुआँ
- शतरंज के खिलाड़ी
नाटक व अन्य
संग्राम, कर्बला, प्रेमा, प्रतिज्ञा, हंस, जागरण (पत्रिका)
प्रेमचंद की विचारधारा
प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने कहा था, ‘साहित्य समाज का दर्पण है।’
उनकी लेखनी में गांधीवादी विचार, ग्रामीण भारत की पीड़ा, वर्गसंघर्ष, स्त्री अधिकार और सांप्रदायिक सौहार्द जैसे मुद्दे बार-बार आते हैं। वे किसी ‘हीरो’ को महिमामंडित नहीं करते, बल्कि छोटे पात्रों के माध्यम से समाज का बड़ा चित्र प्रस्तुत करते हैं।
ऐतिहासिक संदर्भ और महत्त्व
प्रेमचंद स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में सक्रिय थे। गबन और कर्मभूमि जैसे उपन्यासों में उन्होंने आंदोलन की भावना को स्थान दिया। 1936 में उनकी मृत्यु हुई, उसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसमें प्रेमचंद का उद्घाटन भाषण ऐतिहासिक माना जाता है। उन्होंने कहा था èहमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, सामाजिक परिवर्तन है।è
प्रसिद्ध उद्धरण
‘दुनिया में दुख ही दुख है, पर मरने से पहले सुख की आशा कौन छोड़ता है?’
‘ईश्वर के नाम पर मर मिटना आसान है, पर मनुष्य के लिए मरना कठिन।’
‘पढ़ाई का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, आत्मा का विकास होना चाहिए।’
‘हमारे समाज में श्रम की कोई प्रतिष्ठा नहीं।’
तुलसीदास और प्रेमचंद : तुलनात्मक दृष्टिकोण
गोस्वामी तुलसीदास और मुंशी प्रेमचंद दो भिन्न ध्रुवों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन दोनों की लेखनी का उद्देश्य समाज को जागरूक और समरस बनाना था। तुलसीदास ने धार्मिक चेतना को भक्ति के माध्यम से सरल और जन-हितकारी रूप में प्रस्तुत किया, जबकि प्रेमचंद ने सामाजिक कुरीतियों और अन्याय के विरुद्ध कलम चलाई।एक ने भगवान को जनता के करीब लाया, दूसरे ने जनता की पीड़ा को साहित्य के ज़रिए देश के सामने रखा।उनकी जयंती पर उन्हें स्मरण करना केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि यह आत्मावलोकन का अवसर है कि आज का लेखक किस मार्ग पर चल रहा है, तुलसी के भक्ति मार्ग पर या प्रेमचंद के यथार्थ मार्ग पर।